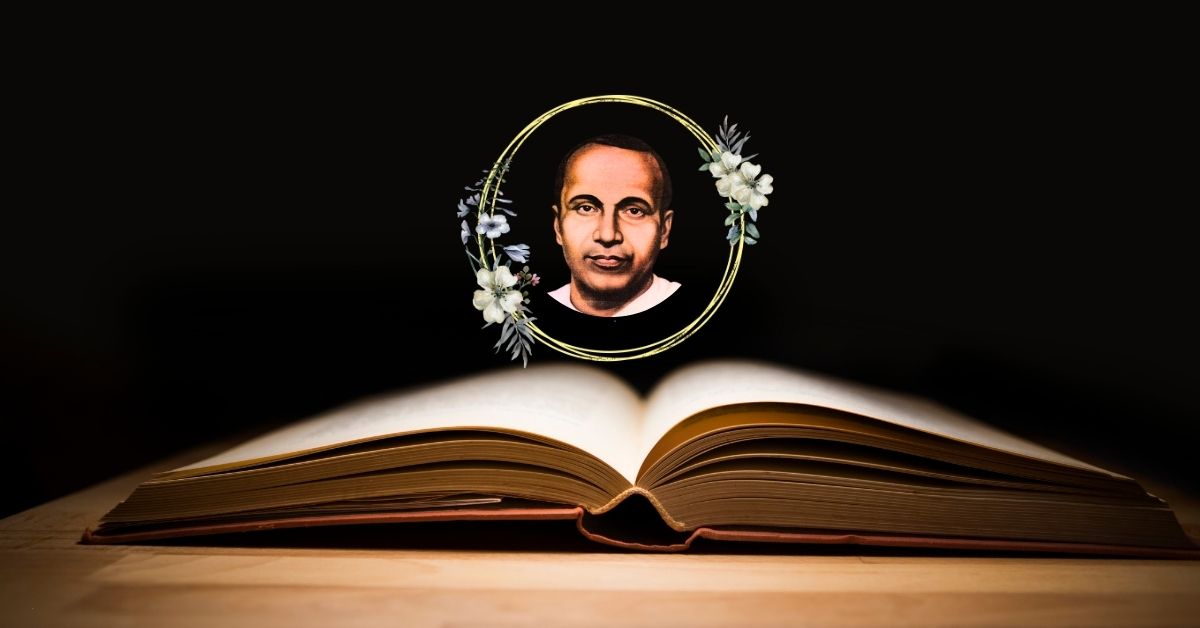लेख का पहला पैराग्राफ पाठकों को आकर्षित करने और विषय से परिचित कराने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए आपको एक दिलचस्प तथ्य, प्रश्न, उद्धरण, या कहानी से शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा, यह स्पष्ट होना चाहिए कि लेख किस विषय पर केंद्रित है और पाठकों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
उदाहरण:
अगर लेख “छायावादी काव्य की विशेषताएँ” पर है, तो पहला पैराग्राफ इस तरह हो सकता है:
“हिंदी साहित्य में छायावाद एक ऐसा युग था, जिसने कविता को सिर्फ बाहरी सौंदर्य से नहीं, बल्कि गहरे आत्मबोध और संवेदनाओं से जोड़ दिया। इस युग के कवियों ने आत्म-अभिव्यक्ति, प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद को अभूतपूर्व ढंग से प्रस्तुत किया। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला जैसे कवियों ने छायावादी काव्य को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। इस लेख में हम छायावाद की प्रमुख विशेषताओं और उसके प्रभावों को विस्तार से समझेंगे।”
ऐसा पहला पैराग्राफ SEO-अनुकूलित भी होगा क्योंकि इसमें मुख्य कीवर्ड (छायावादी काव्य, आत्म-अभिव्यक्ति, प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा) का सही ढंग से उपयोग किया गया है। 😊
छायावादी कविता में आत्म-अभिव्यक्ति, सौंदर्य और प्रकृति चित्रण
1. आत्म-अभिव्यक्ति:
छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में व्यक्तिगत जीवन के गहन भावों और अनुभूतियों को खुलकर अभिव्यक्त किया। सुख-दुःख से भरी कविताओं में आत्मा की गहराइयों को उकेरा गया। जयशंकर प्रसाद की ‘आँसू’ और सुमित्रानंदन पंत की ‘उच्छवास’ इसी का उदाहरण हैं।
पंत जी ने अपनी कविता में प्रेम को एक पूजनीय भावना के रूप में चित्रित किया:
“विधुर उर के मृदु भावों से, तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार।
पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारि, मूँद दुहरे दृग द्वार।।”
वहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ ने ‘राम की शक्ति पूजा’ में अपने संघर्षों और जीवन की निराशा को व्यक्त किया:
“धिक् जीवन जो पाता ही आया है विरोध।
धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध।।”
2. सौंदर्य चित्रण:
छायावादी कवि प्रेम और सौंदर्य के गहरे चितेरे थे। इनका सौंदर्य-चित्रण रीतिकालीन श्रृंगार रस से भिन्न था। इन्होंने प्रेम को बाह्य आकर्षण के बजाय आंतरिक भावनाओं से जोड़कर देखा:
“नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग।
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग।।”
3. प्रकृति चित्रण:
छायावादी कवियों ने प्रकृति को केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के सबसे निकट माना। सुमित्रानंदन पंत ने इसे नारी प्रेम से भी श्रेष्ठ बताया:
“छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया।
बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूँ मैं लोचन।”
प्रकृति केवल मनमोहक नहीं, बल्कि भयावह भी हो सकती है। जयशंकर प्रसाद ने ‘कामायनी’ में प्रकृति के विनाशकारी रूप को उकेरा:
“धू-धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य।
पंचभूत का भैरव मिश्रण, सम्पाओं के सकल निपात।।”
4. प्रकृति और आधुनिक युग:
प्रसाद जी का मानना था कि यदि मनुष्य प्रकृति का संरक्षण करे, तो यह जीवन की रक्षक बन सकती है। लेकिन अति विज्ञानवाद और औद्योगीकरण ने प्रकृति को इतना क्षति पहुँचाया कि अब यह विनाशकारी रूप धारण कर रही है। प्राकृतिक असंतुलन के कारण जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ मानव जीवन को अस्त-व्यस्त कर रही हैं।
नारी चित्रण
आलोचकों ने माना कि छायावाद में प्रकृति और नारी चेतना कवियों की मानसिक धारणा (कल्पना) का रूप लेकर आई। जीवन और समाज में पराधीनता व बन्धनों का दंश झेल रहे इन रचनाकारों ने नारी तथा प्रकृति को आत्म प्रक्षेप (अपने मन से स्वतन्त्र देखने की कोशिश) के रूप में प्रस्तुत किया।
नारी यह सहचरी, सखी तथा प्रेयसी बनकर आई। वह भी सामन्ती बन्धनों में जकड़ी हुई थी। चहारदीवारी में कैद तथा भोग की वस्तु के रूप में नारी यातना ग्रस्त थी। छायावादियों ने नारी शरीर के उच्चावचों की जगह उसके हृदय की अतल गहराइयों पर ध्यान दिया। पन्त जी ने यह स्पष्ट किया कि नारी सिर्फ भोग (सेक्स) का उपकरण नहीं है बल्कि जीवन और समाज का अभिन्न अंग भी है।
योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित ।
छायावादी रचनाकारों ने नारी के प्रेम को पवित्र व पावन गंगा की तरह माना। यह माना कि इससे पुरुष हृदय में पड़ी हुई ग्रन्थियों को भी खोला जा सकता है। पन्त ने इस प्रेम को कामशक्तियों से कोसों दूर माना।
अभी तक तो पावन प्रेम कहलाया नहीं पापाचार।
कोई मुझको आज यह मदिरा हाय गंगा जल की धार।
प्रसाद जी पर यह आरोप लगा कि एक तरफ उन्होंने नारी को श्रद्धा का विषय माना तो दूसरी तरफ उसे मध्ययुगीन पुरुषवादी दृष्टिकोण से भी देखा। “नारी तुम केवल श्रद्धा हो” में विश्वास रखते हुए प्रसाद जी ने इस बात पर ध्यान दिया कि नारी को पश्चिमी बाजारवादी मूल्यों तथा भौतिकवादी आकर्षणों से बचाकर भारतीय संस्कृति की रक्षा की जा सकती है। भारतीय नारीत्व के मूल्य सेवा, समर्पण, त्याग, ममता तथा सतीत्व आदि रहे हैं। नारी इससे जुड़कर ही अपनी मर्यादा तथा समाज की रक्षा कर सकती है।
वेदना या पीड़ावाद
छायावादी रचनाकारों ने स्वतन्त्रता अथवा मुक्ति कामना के उद्देश्य से प्रकृति तथा नारी स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता की बात की। लेकिन वास्तव में स्वतन्त्रता बाधित थी। समाज में जड़ता अभी भी व्याप्त थी, औपनिवेशिक बन्धन भी ज्यों-के-त्यों व्याप्त थे। इन्होंने कल्पनाशीलता के माध्यम से स्वतन्त्रता तलाशने की कोशिश की। परन्तु यथार्थ पूर्णतः पराधीनता से ग्रसित था। ऐसे में वेदना अथवा पीड़ा का उभरना स्वाभाविक था। निराला, प्रसाद, पन्त, महादेवी वर्मा की रचनाओं में इसकी अभिव्यक्ति सभी स्तरों पर दिखाई पड़ती है।
निराला
दुःख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही।
तुझ में पीड़ा को ढूँढा तुझसे ढूँढेंगी पीड़ा।
मैं नीर भरी दुःख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही
कल उमड़ी थी आज मिट चली।
मैंने ‘मैं’ शैली अपनाई, देखा एक दुखी जन भाई। दुःख की छाया पड़ी हृदय में, झट वेदना बन उमड़ आई।।
कल्पनाशीलता
छायावादी कविता का आधार कल्पनाशीलता आलोचकों ने माना। छायावादी रचनाकारों ने कैशोयी भावुकता के कारण कल्पना के ऊँचे-ऊँचे उड़ान भरे उन्होंने कल्पना को ही सृजना का नाम दिया। निराला ने कविता को कानन की देवी कहा, तो पन्त जी ने कल्पना को बिहुबल बाल कहा। उन्होंने लिखा कि कोई भी गम्भीर और व्यापक अनुभूति काल्पनिक ही होती है। छायावाद में कल्पनाशीलता पर आरोप लगाते यह तर्क दिया गया कि यह कविता पलायनवादी है क्योंकि यथार्थ से कटकर सिर्फ कल्पना लोक का सैर करती है। इस प्रकार के आरोप को निराधार माना जा सकता है क्योकि सामाजिक औपनिवेशिक दबाव के कारण कल्पनाशीलता आई परन्तु उसका अर्थ यह नहीं कि यह कविता जन-जीवन व समाज से कटी हुई थी। इन रचनाकारों का उद्देश्य जीवन व संसार को संवारने का ही था।
आह! कल्पना का मधुर यह सुन्दर जगत कैसा होता।
रहस्यात्मकता
साहित्य में रहस्यात्मकता एक संकल्पना है, कोई भी गुप्त या गोपनीय अनुभूति रहस्यात्मक होती है। आचार्य शुक्ल ने अज्ञात के प्रति जिज्ञासा को ही रहस्यवाद का नाम दिया। प्रस्तुत व प्रत्यक्ष विषय से परे कोई भी अनुभूति रहस्यात्मक ही कहलाएगी। आचार्य ने छायावाद पर चर्चा करते हुए लिखा है कि छायावाद विषय-वस्तु की दृष्टि से रहस्यात्मक व शैली के स्तर पर लाक्षणिक है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने छायावाद शब्द पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रकृति तथा मनुष्य के व्यक्त किन्तु सूक्ष्म सौन्दर्य में आध्यात्मिकता छाया का आभास ही छायावाद है। छायावादियों में रहस्यात्मकता दो कारणों से आई, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता बाधित थी, ऐसे में सहज व सपाट कथन का सहारा नहीं लिया जा सकता था परिणामतः रहस्यात्मक, प्रतीकात्मक तथा लाक्षणिक कथन का सहारा लिया गया। निराला ने ‘राम की शक्ति पूजा’ लिखी।
यदि इस कविता के प्रतीकों को उद्घाटित किया जाए तो राम भारतीय आहत जनता के परिचायक हैं, सीता भारत की खोई हुई स्वतन्त्रता है या अस्मिता है। जबकि रावण विदेशी अपहर्ता का, जिसने भारतीय स्वतन्त्रता का हनन किया है। छायावादी कविता में रहस्यवाद का एक दूसरा भी कारण मानां गया। इन सभी रचनाकारों पर दर्शन का प्रभाव रहा है। निराला पर वेदान्तवाद, प्रसाद पर शैवाद्वैत, महादेवी वर्मा पर वेदनावाद और पन्त पर सर्वात्मवाद का प्रभाव है। इस प्रभाव के कारण इस धारा में रहस्यात्मकता उभरी। छायावादियों ने कैशोर्य भावुकता के कारण प्रकृति की सभी जड़-चेतन वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया को देखने की कोशिश की। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा ही इन्हें रहस्यात्मक बनाती है। पन्त, प्रसाद व महादेवी ने पशु, पक्षी, दिन, रात्रि मौसम के सभी तत्त्वों में रहस्यमयी सत्ता को देखने की कोशिश की। पन्त को लगता है कि चिड़िया की बच्ची के कण्ठ में पहली आवाज भरने वाला भी कोई आध्यात्मिक सत्ता है।
प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तुमने कैसे जाना।
कहो कहाँ हे बाल विहंगिनी, सीखा तुमने यह गाना ।।
महादेवी वर्मा दिन-रात, अन्धकार व प्रकाश के प्रत्यावर्तन में भी इसी प्रकार की आध्यात्मिक रहस्यात्मक छवि देखने की कोशिश करती है।
उदाहरण मेरे प्रियतम को भाता है, तम के परदे में आना
छायावाद और राष्ट्रीय जागरण
डॉ. नामवर सिंह ने कहा कि छायावाद सांस्कृतिक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। छायावादी रचनाकारों ने जिस सांस्कृतिक पुनर्स्थान का प्रयोग किया उसका सम्बन्ध राष्ट्रीय जागरण से ही था। प्रसाद तथा निराला ने भारतीय जनमानस पर विदेशी संस्कृति की अनुकरण धर्मिता तथा विलास प्रियता के प्रभाव को खारिज करना चाहा। प्रसाद के नाटकों में इस प्रकार के भाव सहज ही दृष्टिगोचर होते हैं। भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ व निर्दोष पहलुओं का उद्घाटन उनका उद्देश्य था। उनके नाटकों की गीत उदार राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि पर लिखे गए जहाँ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी भारतीय गौरव का गान करते दिखे।
रुन यह मधुमय देश हमारा
जहाँ पहुँच अंजान क्षितिज को मिलता एक सहारा
हिमाद्रि तुंग श्रंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती।
स्वयंप्रभा समुज्वाला स्वतन्त्रता पुकारती ।।
निराला की कविताओं में भी राष्ट्रीय जागरण मुख्य स्वर के रूप में उभरा। उन्होंने भारतीय भूमि को सिंहों की विहार स्थली माना और विदेशी आक्रान्ताओं को सियार के रूप में देखा, जो सिंहों की निद्रावस्था के कारण ही इस क्षेत्र में निर्भय विचरण कर रहे हैं। यदि भारतीय जग जाएँ तो पराधीनता टिक नहीं सकती।
सिंहों की माँद में आया है सियार, जागो फिर एक बार।
छायावादी शिष्य
छायावादी भाव की तरह कविता में भी मुक्ति का आग्रह दिखा, यह कहा जा सकता है कि कथ्य व शिल्प दोनों स्तरों या अवसरों पर छायावादी कविता मुक्ति कामी व बन्धन विरोधी है। पन्त ने इसे स्पष्ट करते लिखा कि
खुल गए छन्द के बन्द, प्रास के रजत पाश।
अब वाणी हुई मुक्त और कविता अयास ।।
छायावाद में छन्दबद्धता की जगह मुक्त छन्द ने ले लिया जहाँ छन्दों के अनुशासन का लिहाज नहीं किया गया। इस धारा की कविता में पारम्परिक अलंकारों की जगह कुछ पुराने व आधुनिक अलंकारों ने ली; जैसे- मानवीकरण अलंकार तथा विशेषण विपर्यय।
Also Read : भारतेन्दु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ / भारतेन्दु युगीन काव्य की विशेषता