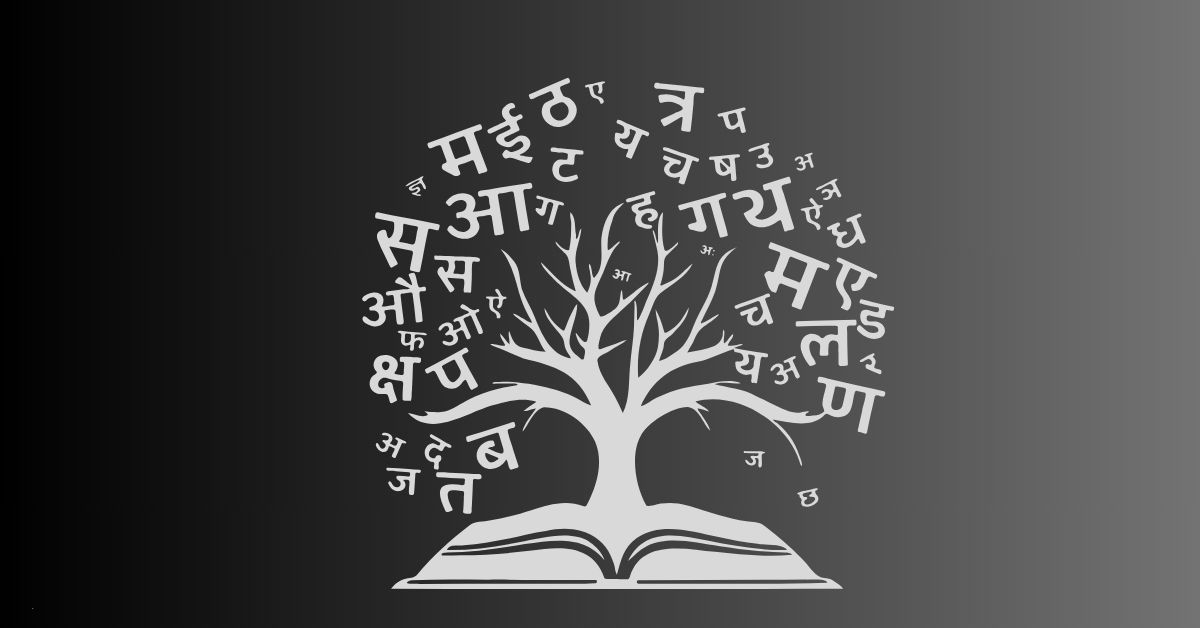हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, जिसे हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन का सूत्रपात माना जाता है। इस परंपरा की नींव फ्रांसीसी विद्वान गार्सी दातासी ने रखी। उन्होंने अपनी रचना ‘इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर ऐन्दुई ऐन्दुस्तानी’ के माध्यम से हिन्दी साहित्य के इतिहास को संरचित किया। यह ग्रंथ दो भागों में विभाजित है, जिनमें पहला भाग 1839 ईस्वी और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
हालाँकि, मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में ‘चौरासी वैष्णवन की वार्ता’, ‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’, और ‘भक्तमाल’ जैसी रचनाएँ मिलती हैं, लेकिन इनमें कालक्रमानुसार विवरण नहीं मिलता, जिससे इन्हें हिन्दी साहित्य के औपचारिक इतिहास ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता।
शिवसिंह सेंगर द्वारा रचित ‘शिवसिंह सरोज’ इतिहास लेखन परंपरा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें लगभग एक हजार कवियों की रचनाएँ और जीवन विवरण शामिल हैं, लेकिन इनमें से कई विवरण संदिग्ध माने जाते हैं। इसके बाद, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ‘द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान’ नामक ग्रंथ की रचना की, जो एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित हुआ। इसे हिन्दी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास माना जाता है, जिसमें केवल हिन्दी कवियों को शामिल किया गया है।
ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ को अधिक प्रमाणिक बनाने के लिए गार्सी दातासी और शिवसिंह सेंगर द्वारा एकत्रित सामग्री का उपयोग किया। इसके अलावा, मिश्र बंधुओं की महत्वपूर्ण कृति ‘मित्रबन्धु विनोद’ भी हिन्दी साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान रखती है। यह एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें 5000 से अधिक कवियों की जानकारी दी गई है। इसकी रचना आठ खंडों में की गई है। रामचन्द्र शुक्ल ने भी इस ग्रंथ से सामग्री संकलित कर रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखा।
हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की यह परंपरा समय के साथ और भी विकसित हुई और इसके आधार पर आधुनिक हिन्दी साहित्य का अध्ययन किया जाने लगा।
हिन्दी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ ( hindi sahitya ke itihas ki lekhan paddhatiyan )
हिन्दी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ को मुख्यतः चार भागों में विभक्त किया गया है ।
- वर्णानुक्रम पद्धति
- कालानुक्रमी पद्धति
- वैज्ञानिक पद्धति
- विधेयवादी पद्धति
वर्णानुक्रम पद्धति
इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्षों के क्रम में दिया जाता है; जैसे- नगेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी (न, ह, क्रम) इस पद्धति में कालक्रम अलग-अलग होने के बाद भी कवि को एक साथ रखा जाता है।
जैसे कबीर व केशव। दोनों का नाम ‘क’ अक्षर से तो है परन्तु कालक्रम भिन्न है। एक का कालक्रम भक्तिकाल तो दूसरे का रीतिकाल है।
डॉ. शिवसिंह सेंगर एवं गार्सी दातासी दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति से लिखे ग्रन्थ अनुपयोगी व दोषपूर्ण माने जाते हैं।
कालानुक्रमी पद्धति
इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथिक्रम से होता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रन्थ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन व मिश्रबन्धुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया है।
वैज्ञानिक पद्धति
वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक पद्धति में क्रमबद्धता तथा तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है।
इस पद्धति भी दोषपूर्ण है क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की माँग करता है। अतः विश्लेषण अनिवार्य है।
विधेयवादी पद्धति
यह पद्धति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इस पद्धति का जन्मदाता तेन था। तेन महोदय ने इस पद्धति को तीन शब्दों में बाँटा है-
1. जाति
2. वातावरण
3. क्षण।
इस पद्धति से इतिहास लिखने की परम्परा की शुरुआत आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने की। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि “प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है।… आदि से अन्त तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है।”
हिन्दी साहित्य के इतिहासकार
हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों में रामचन्द्र शुक्ल जी का नाम अग्रणी है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल
1929 ई. में शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने अपने इस ग्रन्थ में युगीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही। शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को चार खण्डों में बाँटने का प्रयास किया है
1. आदिकाल (वीरगाथा काल)
2. पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल)
3. उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल)
4. आधुनिक काल (गद्यकाल)
शुक्ल जी का यह काल विभाजन अत्यन्त लोकप्रिय हुआ। बाद के इतिहास लेखकों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन एवं कालों का नामकरण प्रस्तुत किया। शुक्ल जी ने ही भक्तिकाल को निर्गुण व सगुण धाराओं में बाँटकर पुनः उन्हें क्रमशः दो-दो उपभागों ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी तथा रामभक्ति व कृष्ण भक्ति में बाँटा। रीतिकाल के कवियों को भी उन्होंने रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त कवियों में स्थान दिया। रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी उन्होंने निष्कर्ष दिए हैं।
आचार्य शुक्ल खोजी प्रवृत्ति के थे। उनकी विवेचना शक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टि थी। यही कारण था कि वे ग्रन्थ की रचना कर पाए जो हिन्दी साहित्य के इतिहास में सुप्रसिद्ध रहा।
डॉ. रामकुमार वर्मा
डॉ. रामकुमार वर्मा जी ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास को दो भागों में प्रकाशित करवाया। जिनमें से एक भाग 1938 ई. में प्रकाशित हुआ।
डॉ. रामकुमार वर्मा जी, शुक्ल जी के वीरगाथाकाल को चारण काल कहना अधिक श्रेष्ठ मानते थे। इससे पहले के साहित्य के लिए उन्होंने सन्धिकाल नाम दिया है।
• डॉ. वर्मा जी ने अपने ग्रन्थ में अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को समाहित किया है। इसी के चलते वे स्वयं को हिन्दी का पहला कवि मानने की गलती कर बैठे।
• डॉ. वर्मा जी के ग्रन्थ का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ है। द्वितीय ग्रन्थ अधूरा है। द्वितीय भाग में भक्तिकाल के बाद के कालों की चर्चा न होने के कारण यह अप्रकाशित है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी
शुक्ल जी के बाद हिन्दी जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निम्न पुस्तकें लिखी हैं जो प्रकाशित हुई हैं
1. हिन्दी साहित्य की भूमिका
2. हिन्दी साहित्य; उद्भव एवं विकास
3. हिन्दी साहित्य का आदिकाल
- शुक्ल जी के वीरगाथा काल को द्विवेदी जी आदिकाल कहना उचित समझते हैं।
- शुक्ल जी ने जिन ग्रन्थों के आधार पर वीरगाथाकाल नाम दिया है, द्विवेदी जी उन ग्रन्थों को प्रामाणिक नहीं मानते।
- शुक्ल जी द्वारा भक्ति आन्दोलन के उदय की व्याख्या का भी द्विवेदी जी खण्डन करते हैं।
द्विवेदी जी की मान्यता है कि भक्तिकाल (हिन्दी सन्तकाव्य) पूर्ववर्ती नाथ, सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। द्विवेदी जी हिन्दी सूफी काव्य को भी संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परम्पराओं पर ही आधारित मानते हैं। कबीर जी की काव्य प्रतिभा को द्विवेदी जी ने उजागर करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया।
डॉ. गणपति ने द्विवेदी जी के योगदान पर लिखा है कि “वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खण्डित किया।” निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिन्दी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार है।
डॉ. गणपति चन्द्रगुप्त
इन्होंने भी हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की परम्परा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। गुप्त जी ने ‘हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास’ दो खण्डों में लिखा है। डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त जी ने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिन्दी साहित्य के इतिहास को तीन खण्डों में विभाजित किया
1. प्रारम्भिक काल
2. मध्य काल
3. आधुनिक काल
डॉ. गुप्त जी ने प्रारम्भिक व मध्यकाल के अन्तर्गत तीन प्रकार के काव्यों की रचना को माना किया है ।
1. धर्माश्रित काव्य
3. राज्याश्रित काव्य
2. लोकाश्रित काव्य
डॉ. गणपति चन्द्रगुप्त जी धर्माश्रित काव्य परम्पराओं के अन्तर्गत पाँच काव्य परम्पराओं को स्वीकार करते हैं
1. धार्मिक रास काव्य परम्परा
2. सन्त काव्य परम्परा
3. पौराणिक काव्य परम्परा
4. पौराणिक प्रबन्ध परम्परा
5. रसिक भक्ति परम्परा
राज्याश्रित काव्य परम्परा के अन्तर्गत भी पाँच काव्य परम्पराओं को स्वीकारा है जो निम्नलिखित हैं
1. मैथिली गीति परम्परा
3. ऐतिहासिक चरित काव्य
2. ऐतिहासिक रास परम्परा
4. ऐतिहासिक मुक्तक परम्परा
5. शास्त्रीय मुक्तक परम्परा
लोकाश्रित काव्य के अन्तर्गत केवल दो परम्पराएँ हैं
1. रोमांसिक काव्य परम्परा
2. स्वच्छन्द प्रेमकाव्य परम्परा
Read More : हिन्दी साहित्य का इतिहास दर्शन और साहित्य के विकास के प्रमुख बिन्दु