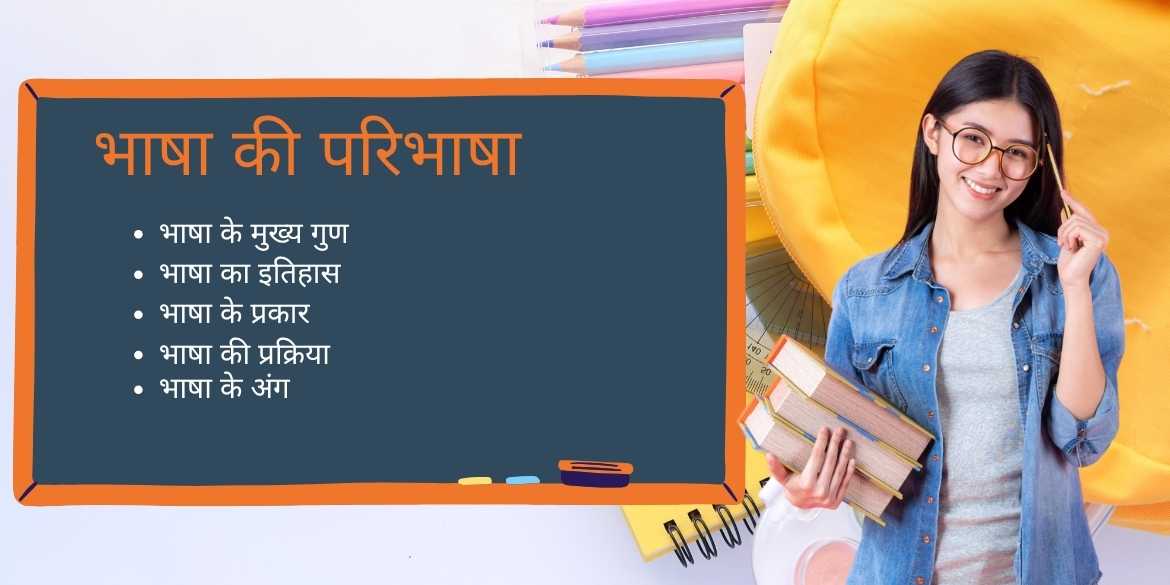भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचार, भाव और जानकारियाँ दूसरों तक पहुँचाते हैं — बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। यह न सिर्फ शब्दों का समूह है, बल्कि अर्थ व्यक्त करने और समझने का एक व्यवस्थित तरीका भी है। सरल भाषा में कहा जाए तो भाषा मनुष्य की सार्थक वाणी है जो सामाजिक व्यवहार और संप्रेषण को संभव बनाती है।
भाषा की परिभाषा (सरल और स्पष्ट)
भाषा उन ध्वनि-चिन्हों, संकेतों और नियमों की प्रणाली है जिनके सहारे व्यक्ति अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुँचाता और दूसरों के विचारों को समझता है। भाषावैज्ञानिकों ने इसे कई तरह से परिभाषित किया है, पर्तुद्ध पर सामान्य बातें यही निकलती हैं:
भाषा ध्वनि-संकेतों पर आधारित होती है।
यह यादृच्छिक (arbitrary) होती है — शब्द और अर्थ के बीच तर्क-संगत प्राकृतिक संबंध ज़रूरी नहीं होता।
यह रूढ़ (परंपरागत) होती है — शब्दों और नियमों का प्रयोग समय व समाज से तय होता आया है।
भाषा के मुख्य गुण (संक्षेप में)
सार्थकता — भाषा को स्पष्ट और अर्थपूर्ण होना चाहिए।
यादृच्छिकता — किसी वस्तु के लिए दिया गया शब्द समाज ने स्वीकार कर लिया तो वह बन गया।
रूढ़ता — शब्दों और प्रयोगों की परंपरा समय के साथ बनती है।
समाज-आधारित — भाषा समाज द्वारा अर्जित और पीढ़ी-दर-पीढ़ी सिखाई जाती है।
भाषा का इतिहास (संक्षेप)
मानव ने शुरुआत में संकेतों और इशारों से संवाद किया — परन्तु पूर्ण विचार संप्रेषित करना कठिन था। धीरे-धीरे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ मिलकर शब्द बनीं और शब्दों के मेल से भाषा विकसित हुई। ‘भाष’ शब्द संस्कृत के ‘भाष्’ धातु से आया है जिसका अर्थ है बोलना।
भाषा के प्रकार
मौखिक (कथित) भाषा: बोलकर किया जाने वाला रूप — बातचीत, भाषण, रेडियो आदि। इसका आधार ध्वनि है और यह अस्थायी होता है।
लिखित भाषा: अक्षरों और चिह्नों के माध्यम से विचारों का स्थायी अभिलेख — पत्र, पुस्तक, समाचार आदि। इसका आधार वर्ण (letters) हैं।
सांकेतिक भाषा: इशारों, संकेतों और संकेत-प्रणालियों द्वारा किया गया संप्रेषण — यातायात संकेत, मूक-बधिरों की भाषा आदि। इसे व्याकरणिक अध्ययन का मुख्य विषय नहीं माना जाता, पर उपयोगी है।
भाषा की प्रक्रिया — कैसे काम करती है?
भाषा संप्रेषण का माध्यम है और इसकी पाँच प्रमुख क्रियाएँ हैं:
सुनना (Listening) — श्रोता का हिस्सा; समझ का आधार।
देखना (Seeing) — दृश्य सामग्री (बोर्ड, स्क्रीन) को पकड़ना।
बोलना (Speaking) — विचारों का मौखिक रूप में प्रस्तुतीकरण।
पढ़ना (Reading) — लिखित संदेश का ग्रहण।
लिखना (Writing) — विचारों का स्थायी रूप देना।
ये प्रक्रियाएँ एक-दूसरे के पूरक हैं और प्रभावी संप्रेषण के लिए सभी ज़रूरी हैं।
भाषा के अंग (संक्षेप)
ध्वनि: मुख से निकलने वाली आवाजें।
वर्ण: मूल स्वर या व्यंजन जो विभाजित नहीं होते।
शब्द: वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है।
वाक्य: शब्दों का संयोजन जो पूर्ण अर्थ दे।
लिपि: मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के चिन्हों का सिस्टम।
भाषा का उद्देश्य और उपयोग
भाषा का मूल उद्देश्य संदेश का संप्रेषण है — विचारों का आदान-प्रदान। इसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताएँ, भावनाएँ (खुशी, दुख, क्रोध, प्रेम), ज्ञान और निर्देश दूसरों तक पहुँचाते हैं। भाषा सामाजिक गतिविधियों, शिक्षा, प्रशासन, साहित्य और व्यापार में अनिवार्य भूमिका निभाती है।
भाषा की प्रकृति — परिवर्तनशीलता
भाषा स्थिर नहीं रहती; यह समय, स्थान और समाज के अनुसार बदलती रहती है। नए शब्द जुड़ते हैं, कुछ शब्द अलग ढंग से उच्चरित होते हैं, और बोलियों के प्रभाव से नई परंपराएँ बनती हैं। यही कारण है कि विश्व में सैकड़ों भाषाएँ और कई लिपियाँ विकसित हुईं — उनका जन्म विकास और विभाजन की प्रक्रिया से हुआ है।
बोली बनाम भाषा — क्या अंतर है?
बोली (Dialect): क्षेत्रीय, सामाजिक या स्थानीय रूप; सीमित क्षेत्र में बोली जाती है; व्याकरणिक मान्यता कम।
भाषा (Language): व्यापक क्षेत्र में प्रयुक्त; अधिकांशतः मानकीकृत व्याकरण और लेखन-परंपरा होती है; प्रशासन, शिक्षा और साहित्य में स्वीकृति मिलती है।
बोलीें किसी भाषा को नए शब्द, मुहावरे और बिम्ब प्रदान करती हैं — कई बार बोली विकसित होकर मानक भाषा बन जाती है (जैसे खड़ी बोली → आधुनिक हिंदी)।
लिपि और भाषा
लिपि वह प्रणाली है जिससे मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाता है। एक भाषा एक से अधिक लिपियों में लिखी जा सकती है और एक लिपि कई भाषाओं के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उदाहरण: हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है; अंग्रेजी रोमन लिपि में। देवनागरी की विशेषता यह है कि इसमें स्वर और व्यंजन का समन्वित लेखन व्यवस्थित है।
मातृभाषा, प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय भाषा
मातृभाषा: वह भाषा जो व्यक्ति अपने परिवार से पहली सीखता है।
प्रादेशिक भाषा: किसी प्रदेश में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा।
अंतर्राष्ट्रीय भाषा: वह भाषा जिसे दो या अधिक देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है (जैसे अंग्रेजी)।
भाषा सुधारने के व्यावहारिक सुझाव
यदि आप अपनी भाषा (बोलने या लिखने) में सुधार चाहते हैं तो इन बिंदुओं पर ध्यान दें:
छोटी-छोटी गलतियों पर नजर रखें और उन्हें सुधारें।
बच्चों की भाषा पर ध्यान दें — शुरू से ही सही आदतें बनें।
नियमित रूप से अच्छी किताबें पढ़ें; नए शब्दों के अर्थ और प्रयोग सीखें।
लिखते और बोलते समय विराम-चिह्न और व्याकरण का ध्यान रखें।
उपयुक्त विशेषण और क्रिया-विशेषण का संतुलित प्रयोग करें।
मुहावरों, लोकोक्तियों और बिंबों का सही प्रयोग सीखें।
उस भाषा का व्यावहारिक व्याकरण समझें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं।
निष्कर्ष
भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक सामाजिक-नियमित प्रणाली है जो विचारों, भावनाओं और सामाजिक क्रियाओं का समन्वय करती है। यह यादृच्छिक, रूढ़ और परिवर्तनशील है। बेहतर संप्रेषण, सम्मान और प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का सतत अभ्यास और अध्ययन आवश्यक है। भाषा सीखना और सुधारना जीवनभर की प्रक्रिया है — और यह प्रक्रिया हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (संक्षेप)
प्रश्न: क्या पशु-पक्षियों की बोलियाँ भी भाषा हैं?
उत्तर: नहीं — उनके संकेतन संप्रेषण हैं, पर मानव भाषा जैसी संरचना, स्मृति और प्रतीक-व्यवस्था नहीं होती।
प्रश्न: भाषा बदलती क्यों है?
उत्तर: सामाजिक संपर्क, अनुकरण, भौगोलिक प्रवास, तकनीकी और सांस्कृतिक प्रभावों के कारण शब्द और प्रयोग बदलते हैं।
प्रश्न: बोली और भाषा में सबसे बड़ा फर्क क्या है?
उत्तर: क्षेत्रीयता और मानकीकरण — बोली सीमित क्षेत्र की होती है; भाषा व्यापक और मानकीकृत होती है।