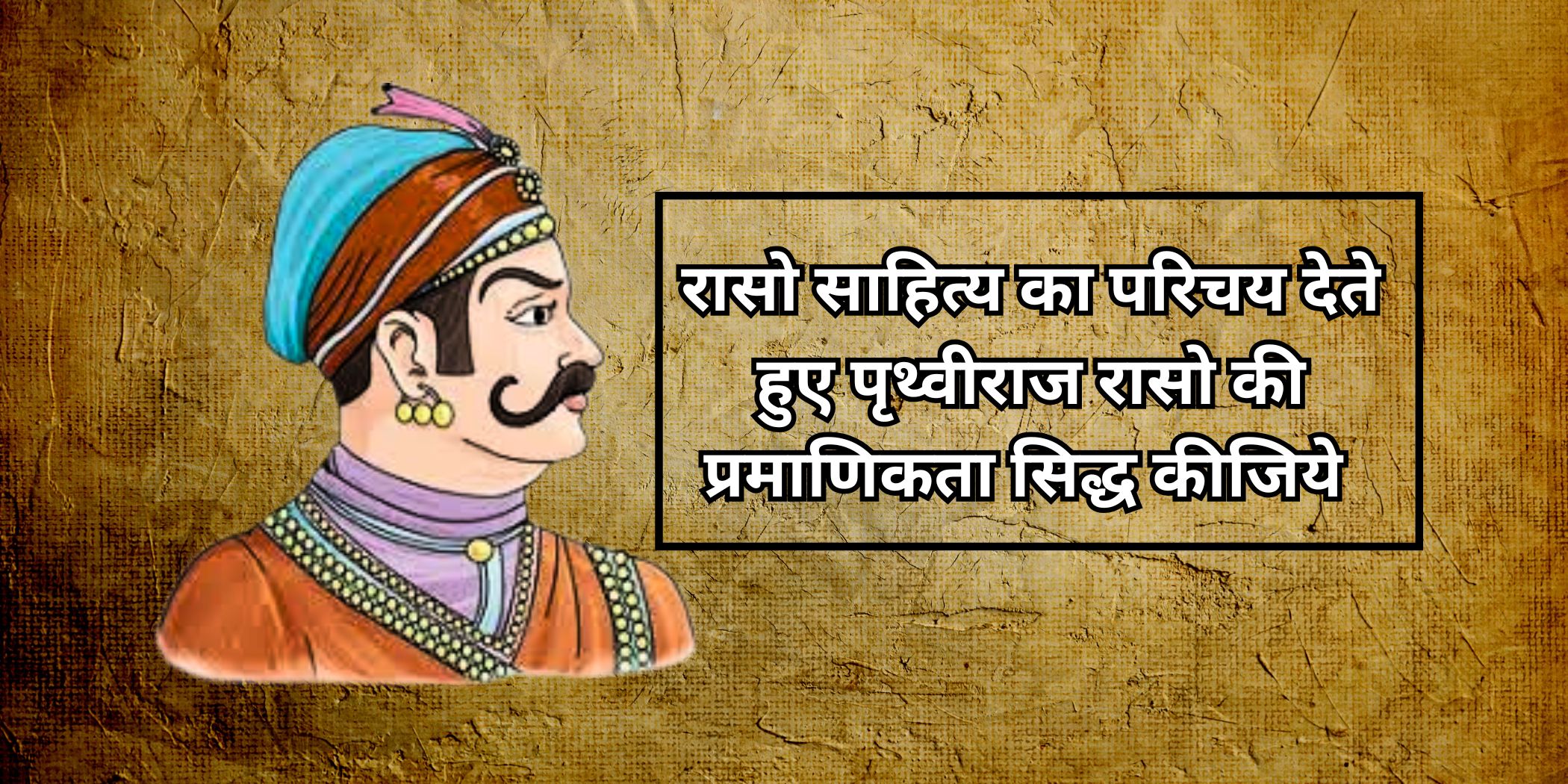साहित्य का निर्माण परम्पराओं से होता है । कोई भी कवि किसी न किसी परम्परा का सहारा लेकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है । हिन्दी साहित्य में प्रत्येक युग किसी न किसी परम्परा का सहारा लेकर निर्मित हुआ है । रासो काव्य- परम्परा भी इसका अपवाद नहीं हैं। रासो की परम्परायें हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काल से प्रारम्भ हुई और निरन्तर निर्बाध रूप से विकसित होती रही। इस परम्परा के बीच-बीच में कतिपय परिवर्तन भी हुए किन्तु वे परिवर्तन ऐसे नहीं थे, जिन्हें मौलिक और विशिष्ट परिवर्तन कहा जा सके ।
हिन्दी परम्परा के आदि कवि
कवि चन्द्रबरदाई का जन्म हिन्दी साहित्य में एक अभूतपूर्व घटना है। उनके आविर्भाव का समय न केवल संघर्षमय था, बल्कि भारी उथल-पुथल और परिवर्तनों का भी समय था। चंद्र बरदाई हिन्दी की परम्परा के आदि कवि और अपभ्रंश परम्परा के अंतिम कवि थे। रासो का विकास अपभ्रंश परम्परा में हुआ और उसकी परम्परा आधुनिक युग तक बराबर चली आ रही है। हिन्दी को जो रासो परम्परा प्राप्त हुई, वह गुजराती से आई है। रासो परम्परा में प्रथम रासो ग्रंथ संदेश रासक है, जिसकी रचना अब्दुल रहमान ने की बताई गई है ।
सन्देश रासक
रासो साहित्य के शोधकर्ताओं और प्राचीन के समीक्षकों की धारणा रही है कि रासो परम्परा का श्री गणेश अब्दुल रहमान की कृति से हुआ है । विद्वानों की मान्यता है कि रासो परम्परा में प्रथम प्रमाणिक कृति सन्देश रासक ही है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इसका रचना काल वि. 11 वीं शताब्दी माना है। मुनि जिन विजय के अनुसार उसकी रचना 12 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 13 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में स्वीकार की है। इस ग्रंथ की कहानी बड़ी सरस और मार्मिक है। इसमें प्रोषितपतिका नायिका के विरह का मार्मिक वर्णन मिलता है इसकी नायिका पथिक के माध्यम से अपने पति के पास प्रेम-सन्देश भेजती है। सन्देश का ऋतु वर्णन बड़ा ही मार्मिक है ।
मंजु रास
डॉ. विपिन बिहारी त्रिवेदी की मान्यता है कि संदेश रासक से पूर्व मंजु रास नामक ग्रंथ मिलता है। इसमें मालवा के शासक मंजु और कर्नाटक के तैलप की बहिन मृणालवती के प्रेम का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के कतिपय छन्द ‘सिद्धहेमशब्दानुशासन’ और मेरुतुंग के प्रबन्ध चिंतामणि में भी प्राप्त होते हैं ।
भरतेश्वर बाहुबली रास
शालिभद्र द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास भी एक महत्त्वपूर्ण रचना के रूप में प्राप्त होता है । यह रासो वीर रसात्मक है । इसमें ऋषभ के भवतेश्वर और बाहुबली दो पुत्रों के युद्धों का वर्णन किया गया है । इसका रचना काल संवत् 1241 स्वीकार किया गया है। शालिभद्र ने ही बुद्धिरास भी लिखा । इसी समय लिखे गये रासो काव्यों में कवि आसगु कृत जीवदया राम तथा चन्दनबाल राम कवि देल्हणकृत जयसुकुमाल रास, जीवंधन कृत मुक्तावलि रास व उपदेश रसायन रास का नाम विशेषत उल्लेखनीय है ।
उपदेश रसायन रास
रासो प्रायः वीर रसात्मक रहे हैं, आपवादिक रूप से कतिपय ऐसे रासो ग्रंथ भी लिखे गये हैं, जो वीरभावेतर पद्धति पर लिखे गये हैं, जिन दत्तसूरि ने उपदेश रसायन की रचना की है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस कृति को वीर काव्य परम्परा की कोटि में नहीं स्वीकार किया जा सकता है । इसका कारण इस ग्रंथ का नीति-काव्य शैली में लिखा होना है। नीति काव्य शैली के साथ-साथ इसमें जैन धर्म सम्बन्धी सामग्री की प्रधानता है ।
डिंगले में रासो ग्रंथ
इस परम्परा में जो रासो ग्रंथ मिलते हैं, उनमें प्रायः चरित्र की ही प्रधानता रही। इस परम्परा में आने वाली रचनाओं में ऐतिहासिक तत्त्वों की रक्षा नहीं की गई है। इनके आकार-प्रकार, विषय-वस्तु और वर्णन-शैली में प्रर्याप्त विभिन्नता है । 12 वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच रासो परम्परा का पर्याप्त विकास हुआ है ।
इस अवधि में लिखे गए रासो या रास-ग्रंथ निम्नांकित हैं-
(1) बीसलदेव रासो,
(2) जम्बू स्वामी रास,
(3) रेवन्तगिरि रास,
(4) कच्छुनि रास,
(5) गौतम रास,
(6) दशाण भद्र रास,
(7) वस्तुपाल तेजपाल रास,
(8) श्रेणिक रास,
(9) पेपड़ रास,
(10) समरसिंह रास,
(11) सप्तक्षेत्रि रास,
(12) चन्दनबाला रास ।
इन रासों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है-
बीसलदेव रासो
बीसलदेव रासो, रासो परम्परा का प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता नरपति नाल्ह माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार यह ग्रंथ वीरगीत के रूप में सबसे प्राचीन है। इसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास भी मिलता है। कपितय विद्वानों की दृढ़ धारणा है कि इसको वीर काव्य परम्परा का ग्रंथ न मानकर प्रेम गीत परम्परा का ही मानना चाहिए। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें वीर भावों का चित्र नहीं के बराबर है। डॉ. हरिहरनाथ टण्डन के शब्दों में, इस ग्रंथ में कवि ने प्रेम और विरह के मधुर चित्र खींचे है। वियोग का चित्रण अत्यन्त मार्मिक है । कवि की सहृदयता और भावुकता का दिग्दर्शन राजमती का विरह ही है। कलापक्ष का निर्वाह कवि ने अच्छी तरह नहीं किया है। छंद-दोषों का तो बहुल्य है ।
17 वीं 18 वीं शताब्दी के रासो ग्रंथ का पता उस समय लगा जबकि पण्डित मोतीलाल मेनारिया नरोत्तम स्वामी और डॉ. दशरथ शर्मा व श्री अगरचन्द्र नाहटा ने हस्तलिखित प्रतियों को खोज निकाला । 17 वीं शती के रासो ग्रंथों की नामावली इस प्रकार है-(1) कुमारपाल रास रचयिता ऋषभदास, (2) राम रासो रचयिता माधोदास, (3) विनोद रासो रचयिता सुमतिहंस । अठारहवीं शताब्दी के रासो ग्रंथों के नाम इप्स प्रकार है-(1) छत्रसाल रासो रचयिता डूंगरसी, (2) संगतसिंह रासो रचयिता गिरिधर चारण, (3) खुम्मान रासो रचयिता दलपति विजय । 19 वीं शताब्दी में जिन रासो ग्रंथों का पता चला है उनमें श्रीपाल रास विशेष उल्लेखनीय रचना है । 18 वर्वा शताब्दी के रासो ग्रंथों में खुम्मान रासो को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है।
खुम्मान रासो
इस रासो के रचयिता के रूप में दलपति विजय का नाम प्रसिद्ध है। इन्हें दौलत विजय भी कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में मेवाड़ के खुम्मान अथवा सूर्यवंश की महत्ता का वर्णन किया गया है-
कवि दीजै कमला कला, जोड़णा कवित जुगति । सूरजि बंस तणौ सुजस, वरणन करूँ विगति ।।
यह एक भावात्मक रचना है। अतः रसोत्कर्ष की व्यंजना के आधार पर इस रासो को मधुर एवं कोमल भाव-परम्परा में ही स्थान प्राप्त हो सकता है। इसके संबंध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन है कि “यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है, उनमें कितना अंश पुराना है। इसमें महाराज प्रतापसिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है, वह वि.सं. 17 वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ होगा। यह नहीं कहा जा सकता. है कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके परिशिष्ट का ।” श्री मोतीलाल मेनारिया का कथन है कि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर विचार किया जाय तो यही तथ्य सामने आते हैं कि दलपति तपागच्छीय जैन साधु शंति विजय के शिष्य थे और दीक्षा के बाद उन्होंने अपना नाम दौलत विजय रख लिया था । यह ग्रंथ आठ खण्डों में विभक्त है। इसकी भाषा पिंगल है ।
हास्य मिश्रित रासो ग्रंथ
रासो काव्य परम्परा में हास्य-मिश्रित रासो ग्रंथों को भी नहीं भुलाया जा सकता है। इस वर्ग में आने वाले ग्रन्थों में मकाड़ रासो, ऊंदर रासो, खीचड़ रासो और गोधा रासो आदि हैं। ये सभी रासो ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखे गए हैं।
पिंगल या बृजभाषा के रासो ग्रंथ
डिंगल के रासो ग्रंथों की जो परम्परा मिलती है, वैसी ही परम्परा पिंगल के ग्रंथों की भी मिलती है। पिंगल या ब्रजभाषा में लिखे गए रासो ग्रंथों की नामांवली इस प्रकार है-
(1) हम्मीर रासो (शारंगधर कृत),
(2) परमार रासो (जगनिक कृत),
(3) विजयपाल रासो (निल्लहसिंह भट्ट कृत),
(4) काहिया को रासो (गुलाब कवि कृत),
(5) कायम रासो (जानकवि कृत),
(6) रतन रासो (जोधराज कृत),
(7) बुद्धि रासो (जल्हकवि कृत),
(8) राउजैतसी रौ रासो (अज्ञात) ।
इन रासो ग्रन्थों का विशेष महत्व है-हम्मीर रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-
हम्मीर रासो
यह ग्रंथ देशी भाषी का वीरगाथात्मक महाकाव्य बताया गया है। यह अनुपलब्ध है-इसके विषय में आचार्य शुक्ल का यह अभिमत है-‘प्राकृत पिंगल सूत्र में कुछ पंद्य असली हम्मीर रासो के हैं ।”
परमाल रासो
जगनिक को इसका रचयिता स्वीकार किया गया है। वे कालिंजा के राजा परमाल के चारण और राजकवि थे। यह ग्रंथ आल्हाखण्ड नाम से भी प्रसिद्ध हैं। लोक-वीरगाथा के रूप में इसका विकास लोकगायकों द्वारा होता रहा है। सन 1882 ई. में सर चार्ल्स इलिट ने अनेक भाटों की सहायता से इसका सम्पादन करवाया था। यह वीर रसात्मक काव्य है, इसका आधार पृथ्वीराज रासो का महोबा समय है। डॉ. सुन्दरदास की मान्यता है कि जिन प्रतियों के आधार पर यह संस्करण सम्पादित हुआ है, उनमें यह नाम नहीं है।
उनमें चन्द्रगुप्त पृथ्वीराज रासो का महोबा खण्ड लिया गया है। किन्तु वास्तव में यह पृथ्वीराज रासो का महोबा खण्ड नहीं है, वरन् उसमें वर्णित घटनाओं को लेकर मुख्यतः पृथ्वीराज रासो में दिए हुए एक वर्णन के आधार पर लिखा हुआ एक स्वतंत्र ग्रन्थ है । यद्यपि इस ग्रन्थ का नाम मूल प्रतियों में पृथ्वीराज रासो दिया हुआ है, पर इस नाम से इसे प्रकाशित करना लोगों को भ्रम में डालना है। अतएव मैंने इसे परमाल रासो नाम देने का साहस किया है “खैर, इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता की बात यदि छोड़ दी जाय तो यह बात निस्संकोच भाव से स्वीकार की जा सकती है कि इसमें कवि की हृदयस्पर्शी भावधारा अजस्र गति से प्रवाहित होकर आज तक रसिकों के मन को आप्लावित करती आई-कवि के लिए यह कम महत्त्व की बात नहीं ।”
विजयपाल रासो
इस ग्रंथ के रचयिता नल्लसिंह भट्ट माने जाते हैं, जो विजयपाल के दरबारी कवि थे। हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों ने इसका रचना काल वि. 1100 (सन् 1043) माना है। इतने पर भी यह सच लगता है कि अपने वर्तमान रूप से यह 16 वीं शताब्दी की रचना प्रतीत होती है। इस ग्रंथ में विजयपाल की विजय यात्राओं का वर्णन है। यह वीर रसात्मक रचना है। यों तो इसके 42 छन्द उपलब्ध है फिर भी इसके महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है ।
यही रासो काव्यों की परम्परा है। इस पर विचार करते हुए डॉ. माताप्रसाद गुम ने निम्नांकित महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष दिए हैं-
(1) रास तथा रासो नाम में कोई भेद नहीं है। दोनों नाम एकार्थक है और कभी-कभी एक ही साथ प्रयुक्त हुए हैं ।
(2) रासो के अन्तर्गत प्रबन्ध की दो धारायें-दो विभिन्न परम्परायें आती है। एक तो गीत नृत्य परक है और दूसरी छन्द वैविध्य परक । पहली का उद्भव कदाचित नाट्य रासकों से हुआ है और दूसरी रासक या रासा बन्ध से । दोनों परम्पराओं को मिलाया नहीं जा सकता है ।
(3) गीत-नृत्य परक परम्परा की रचनाएँ आकार में प्रायः छोटी होती है। क्योंकि उन्हें स्मरण करना पड़ता है, जबकि छन्द-वैविध्यपरक परम्परा में रचनायें छोटी बड़ी सभी आकारों की है।
(4) गीत-नृत्य-परक परम्परा का प्रकार जैन धर्मावलम्बियों में अधिक रहा है। उनके रचे हुए प्रायः समस्त रासो इसी परम्परा में हैं। दूसरी परम्परा का प्रचार जैनेतर समाज में विशेष रहा है अब यह प्रमाणिक हो चुका है कि इनका भी अभिनयात्मक गायन होता रहा है।
(5) जैन रचनाओं की भाषा बहुत पीछे तक अपभ्रंश बहुत रही है, जबकि अन्य रचनाओं की भाषायुगीन बातचीत की भाषा हो गई थी ।
(6) गीत-नृत्य-परक रासो रचनायें प्रायः पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में लिखी गई थी, जबकि छन्द वैविध्य परक रासकों की रचना सम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश में हुई है।
(7) काव्य की दृष्टिकोण दूसरी ही परम्परा में प्रधान रहा है, प्रथम में नहीं और इसी कारण शुद्ध साहित्य की दृष्टि से दूसरी परंपरा अधिक महत्त्व रखती है। इसी कारण तो आचार्य शुक्ल ने उन्हें वीरगाथात्मक कहकर वीरगाथा काल के अन्तर्गत गिनाया है ।
(8) चरित्र तथा काव्य धाराओं के समान ही यह रासो काव्यधारा भी साहित्य की एक समृद्ध काव्यधारा रही हैं, इसका गम्भीर अध्ययन नितान्त अपेक्षित है और हमेशा रहेगा ।
यही रासो-काव्य-परम्परा के ग्रन्थों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यही रासो काव्यों की परम्परा है। और यही परम्परा निर्बाध रूप से एक सुदीर्घ अवधि तक गतिमान रही है ।
पृथ्वीराज रासो का ध्यान
यह तो निर्विवाद सत्य है कि रासो-काव्य-परम्परा में पृथ्वीराज रासो का स्थान और महत्त्व सर्वोपरि है। एक प्रकार से कृष्ण भक्तिधारा में जो स्थान सूरदास के सूरसागर का है, राम भक्तिधारा में जो महत्त्व तुलसी के रामचरितमानस को प्राप्त है, वही महत्त्व रासो-काव्य परम्परा में पृथ्वीराज रासो को प्राप्त है। अनेक विद्वानों ने इस कृति को हिन्दी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिन्दी का प्रथम महाकाव्य माना है, तो स्वर्गीय गुलाबराय ने स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना है और मोतीलाल मेनारिया ने इसमें महाकाव्य की भव्यता और दृश्य-काव्य की संजीवता देखी है। डॉ. विपिन बिहारी ने कतिपय त्रुटियाँ के होते हुए भी हिन्दी के इस प्रबन्ध काव्य को निर्विवाद रूप से महाकाव्य सिद्ध करने में कुछ उठा नहीं रखा है।
इसके विपरीत डॉ. श्यामसुन्दर दास ने इसे महाकाव्य नहीं माना है। उनका मत है कि इसमें न तो कोई प्रधान युद्ध है और न किसी महान परिणाम का उल्लेख ही है। सबसे प्रधान बात तो यह है कि इस रासो में घटनाएँ एक दूसरे से असम्बद्ध हैं तथा
कथानक भी शिथिल और अनियमित है, महाकाव्यों की भाँति न तो किसी एक आदर्श में घटनाओं का संक्रमण होता है और न अनेक कथानकों की एकरूपता ही प्रतिष्ठित होती है। डॉ. उदयनारायण तिवारी ने इसे महाकाव्य नहीं माना है-रासो को एक विशालकाय वीर काव्य-ग्रन्थ कहना ही उचित है। स्थान-स्थान पर इसके कथानक में शिथिलता है । पृथ्वीराज रासो की महता और विशिष्टता के अनेक कारण है, जो इस प्रकार है-
(1) पृथ्वीराज रासो में आये वस्तु वर्णन आकर्षक हैं। उनमें विविधता, विभिन्नता और सरसता है ।
(2) रासो में प्रकृति-चित्रण की छटा भी पूरी अद्वितीयता से संयुक्त हैं ।
(3) पृथ्वीराज रासो वीर काव्य है फिर भी उसमें यथावसर वीर रूप के साथ ही रौद्र, भयानक और वीभत्स रस का चित्र तो मिलता ही है, श्रृंगार को भी चित्रित किया गया है।
(4) कलात्मकता की दृष्टि से भी पृथ्वीराज रासो अप्रतिम कृति है । उसकी भाषा मिश्रित है, उसकी अलंकार-योजना विशिष्ट है । रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग कृति को अत्यधिक आकर्षक बनाने में सफल हुआ है ।
(5) यों तो विद्वानों ने चन्द कवि को छप्पय का सम्राट माना है। यह तो सच ही है कि चन्द कवि के छप्पय जितने सरस, स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक है, उतने अन्य किसी वीर काव्य में नहीं हैं। पृथ्वीराज रासो में 72 छन्दों का प्रयोग कवि की प्रतिभा को उदाहत करता है ।
निष्कर्ष
यद्यपि रासों की परम्परा में पृथ्वीराज रासो सर्वोपरि है । तथापि उसकी प्रमाणिकता-अप्रमाणिकता को लेकर पर्याप्त विवाद हिन्दी जगत में रहा है । यदि इस प्रश्न को उपेक्षित कर दिया जाय तो इसके काव्य-सौष्ठव के आधार पर ही इस ग्रन्थ के महत्त्व को आँका जा सकता है । वस्तुतः यह ग्रन्थ कवि की प्रौढ़ अनुभूति और उर्वरा कल्पना-शक्ति का प्रमाण है। इतिहास और कल्पना के मणिकांचन योग से समुन्नत यह ग्रन्थ उत्कृष्टता का द्योतक है। डॉ. द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इस ग्रंथ के महत्त्व और रासो परम्परा में योगदान को इन शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है- “यह ग्रन्थ राष्ट्रीय भावों को उद्बुद्ध करने गाथा वीर भावनाओं को जागृत करने की महती प्रेरणा में लिखा गया है । इसलिए इस महाकाव्य की महत्ता अक्षुण्ण है । इसका गौरव चिरस्थायी है, इसका प्रभाव शाश्वत है और इन सभी विशेषताओं का मूल कारण इसकी अद्वितीय काव्य-सौष्ठव है जो अत्यन्त उन्नत और उच्चकोटि का है।” अधिकांश समीक्षकों ने इसकी महत्ता को खुले मन से स्वीकार किया है।